








 लिखने के नाम पर आखिरी पोस्ट मैंने 3 तारीख को लिखी थी। उसके बाद घर और ऑफिस के बीच दौड़ लगाती थोड़ी मोहलत का इंतजार कर रही थी कि कब मौका मिले और मैं इलाहाबाद की रंग-रौशनी पर थोड़ी और नजरें घुमाऊं। लेकिन मोहलत कहां है। इतने दिन हुए, दोस्तों ने टोकना भी शुरू कर दिया। अरे इलाहाबाद स्टेशन पर उस चार साल के छोकरे को ऐसी इमबैरेसिंग पोजीशन में बिठाकर आप कहां खिसक लीं। बेचारा बच्चा बैठे-बैठे थक न गया होगा। वो हगकर चुका हो तो मोहतरमा किस्से को आगे बढ़ाइए। मैं भी बच्चे के दुख से कातर बस कलम उठाने ही वाली थी कि दो मुसीबतें मेरे घर पर आ धमकीं। रविवार की छुट्टी मैंने सोचा था, इसी कलमघसीटी के नाम होगी लेकिन जैसाकि जिंदगी में कितना कुछ होना बचा ही रह जाता है, सो यह भी बचा ही रह गया। बच्चे को थोड़ी देर और उसी गफलत में छोड़कर मैं रविवार को धमकीं इन दो मुसीबतों के किस्सा सुनाती हूं।
लिखने के नाम पर आखिरी पोस्ट मैंने 3 तारीख को लिखी थी। उसके बाद घर और ऑफिस के बीच दौड़ लगाती थोड़ी मोहलत का इंतजार कर रही थी कि कब मौका मिले और मैं इलाहाबाद की रंग-रौशनी पर थोड़ी और नजरें घुमाऊं। लेकिन मोहलत कहां है। इतने दिन हुए, दोस्तों ने टोकना भी शुरू कर दिया। अरे इलाहाबाद स्टेशन पर उस चार साल के छोकरे को ऐसी इमबैरेसिंग पोजीशन में बिठाकर आप कहां खिसक लीं। बेचारा बच्चा बैठे-बैठे थक न गया होगा। वो हगकर चुका हो तो मोहतरमा किस्से को आगे बढ़ाइए। मैं भी बच्चे के दुख से कातर बस कलम उठाने ही वाली थी कि दो मुसीबतें मेरे घर पर आ धमकीं। रविवार की छुट्टी मैंने सोचा था, इसी कलमघसीटी के नाम होगी लेकिन जैसाकि जिंदगी में कितना कुछ होना बचा ही रह जाता है, सो यह भी बचा ही रह गया। बच्चे को थोड़ी देर और उसी गफलत में छोड़कर मैं रविवार को धमकीं इन दो मुसीबतों के किस्सा सुनाती हूं। इससे पहले कि मुझे घर और दफ्तर की मारामारी के बीच कुछ कलमघसीटी की फुरसत मिले, ये कविता गौर फरमाएं।
इससे पहले कि मुझे घर और दफ्तर की मारामारी के बीच कुछ कलमघसीटी की फुरसत मिले, ये कविता गौर फरमाएं।
जिदंगी और अनुभवों की दुनिया में एक लंबा अरसा गुजार लेने के बाद अपने उस शहर को देखना, जिसने आपका बुनियादी संस्कार और मानस गढ़ा हो, जिसने दिमाग और हिम्मत के शुरुआती तेवर से लेकर बिजबिजाती हुई भावुकता तक से नवाजा हो, उस शहर को हम किस निगाह से देखेंगे? शहर को देखने की दोनों निगाहें हो सकती हैं। ब्लॉगर मीट में मैंने कहा, यह शहर बिलकुल नहीं बदला। बोधि ने तुरंत प्रतिवाद किया। बोले, यह शहर बहुत बदल गया है। क्या सही है और क्या गलत? दोनों ही नजरें सही हैं शायद। स्टेशन से बाहर निकलकर घर जाने के लिए ऑटो पकड़ा तो सिविल लाइंस की जिन सड़कों से होकर गुजरी, उनकी शक्ल मेरे बचपन की शक्ल से मामूली सा ही मेल खाती थी। शायद यही आधुनिक विकास की एकरूपता है। अब शायद हर शहर का एक पॉश इलाका ऐसा है, जो तेजी से उन्नत रहे सभी शहरों में कमोबेश एक जैसा है। बिलकुल वैसा ही मैकडोनल्डस, जैसा मुंबई में है या इंदौर में या किसी और शहर में। वैसी ही पारदर्शी कांच वाली चमचमाती हुई दुकानें, मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर, नए-नए रेस्टोरेंट, रिलायंस फ्रेश, शहर की हर सड़क, गली दीवारों पर पटे हुए टाटा, वोडाफोन, रिलायंस, मूड्स कंडोम और दुनिया को बदल देने वाले आइडियाज के विज्ञापन। वही चमकती शक्लें। ये मेरे पहचाने हुए शहर की शक्ल नहीं है। तो इस शहर की थकी हुई स्थिरता से बेचैन न होने के लिए यह बदली हुई रौशनीदार रंगत क्या काफी नहीं है? सच ही तो कहा था, शहर बहुत बदल गया है।
लेकिन उसी सिविल लाइंस में आज भी भैंस बीच सड़क में खड़ी होकर टै्फिक रोक देती है और लोग रोज-रोज भैंसों की आवाजाही का कोई स्थाई हल ढूंढने के बजाय भैंस को बीच सड़क में आराम फरमाता छोड़ शॉर्टकट निकालते हैं और साइड से निकल लेते हैं। टै्फिक की दिशा ही मुड़ जाती है और अब वह बीच सड़क के बजाय साइड से निकलने लगती है। कंडोम के सार्वजनिक विज्ञापनों ने भैंसों की विचार प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं डाला है। शहर वालों की प्रक्रिया पर डाला हो तो पता नहीं।
आज भी वहां इंसान द्वारा खींचा जाने वाला साइकिल रिक्शा चलता है। लोग वैसे ही हैं। बड़ी फुरसत में बैठे होते हैं और आने-जाने वाली हर लड़की को तब तक घूरते रहते हैं जब तक वो आंखों से ओझल न हो जाए। चलते हुए कोहनी मार जाते हैं। गाड़ी से हों तो आगे निकल चुकने के बाद भी पलट-पलटकर देखते रहते हैं। पार्किंग में खड़ी स्कूटर पर बड़े सुभीते से पान खाकर थूकते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सफेद स्कूटर पर लाल पीक की सजावट शोभायमान होती है।
एक दिन मैं टैंपो से सिविल लाइंस से गोविंदपुर जा रही थी। दिन का समय था। शिवकुटी के पास टैंपो रुकी। उलझे बालों और कोहड़े जैसी भारी नाक वाला एक आदमी उतरा। इसलिए नहीं कि उसे वहां उतर जाना था। उतर तो दूसरे यात्री रहे थे। मिस्टर कोहड़ा उतरे, सामने एक दुकान थी, जिसका शटर बंद था। उसने दुकान की तरफ मुंह किया और पैंट खोलकर वहीं टैंपो, आती-जाती सड़क और टैंपो के अंदर बैठी दो लड़कियों के सामने प्रकृति की पुकार पर “मैं आया, मैं आया” करते हुए लघु शंकाओं से निपटने लगा। सब नजारा देख रहे थे। टैंपो वाला भी मजे से इंजन घर्र-घर्र करते हुए कोहड़ा महाशय के निपटने और लौटने का इंतजार कर रहा था। मजे की बात ये कि उसके बाद मुश्किल से सौ कदम की दूरी पर कोहड़ा ने टैंपो रुकवाया और उतरकर वहीं सड़क पर ही बने हुए एक मकान का गेट खोलकर अंदर चले गए। कमाल है। ये दो मिनट इंतजार नहीं कर सकते थे? हगने-मूतने के लिए सड़क है और गोभी का पराठा चाभने के लिए घर।
कोई तर्क दे सकता है कि हो सकता है बहुत जोर से आ रही हो। हो सकता है मिस्टर कोहड़ा को लगा हो कि अभी ही नहीं उबरे तो शायद कभी न उबर पाएं। लेकिन ये तर्क देने वालों को अपने ही तर्क पर शर्म आ सकती है, जब वो देखेंगे कि इस शहर में कितने सारे लोगों को अचानक बहुत जोर से आती रहती है। शहर में इधर-उधर लघुशंकाओं से निपटने के नजारे प्राय: देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, अपने ही मुहल्ले में आपको ऐसे नजारे भी दिख सकते हैं कि कोई आदमी अपने घर से बाहर निकले, मोहल्ले की सड़क पार करे और फिर वहीं नाली में पद्मासन की मुद्रा में समस्त शंकाएं निपटाकर घर में वापस घुस जाए। रसूलाबाद में एक आदमी तब मुझे अकसर ऐसा करता दिखता था, जब मैं छठी कक्षा में पढ़ती थी। उसका घर सामने था, लेकिन मूतने के लिए उसे खुले आसमान और आते-जाते लोगों चेहरों की दरकार होती थी। फाफामऊ में एक बार एक लड़का घर से निकला, मुश्किल से पचास कदम गया और एक की पॉइंट पर जाकर, जहां से भीड़ गुजर रही थी, सड़क पर खड़ा होकर पेशाब करने लगा। तब मैं छोटी थी। आज जिस पर मैं इतने शब्द खर्च कर रही हूं, बचपन में यह छवियां मेरे मानस में वैसे ही थीं, जैसे झाडू लगाती मम्मी, सड़क पर टहलते कुत्ते और गाय। बिलकुल सामान्य। इसे देखकर मुझे कुछ विचित्र नहीं लगता था क्योंकि बचपन से मैं ऐसे मनोहारी नजारों को देखते हुए ही बड़ी हुई थी।
 इस बार कुछ चार बरस बाद मेरा इलाहाबाद जाना हुआ। इलाहाबाद – वह शहर जहां मैं पैदा हुई, जहां मैंने जिंदगी के बीस बरस गुजारे। वह शहर, जहां से मेरे सुख-दुख की, हंसी और विषाद की, निजी और सामाजिक करुणा और अपमान की और पहले प्यार की सादगी और बेचारगियों की ढेरों स्मृतियां गुंथी हुई हैं। नौ साल हुए, इलाहाबाद से रोजमर्रा का वह नाता टूट गया। इधर-उधर भटकती, अपनी पहचान और जमीन तलाशती जिंदगी में फुरसत नहीं थी अपने शहर तक लौटकर जाने की। लेकिन कई बार अवसाद और अकेलेपन के बेहद निजी क्षणों में मैंने बहुत भावना से भरकर अपने शहर को याद किया था। पर इस बार बचपन की जानी-पहचानी गलियों को देखना, उनसे गुजरना बड़ा विचित्र अनुभव था। किसी भावुक आवेग और उछाल से भर देने वाला नहीं, अपने अकेलेपन में और ज्यादा धंसा देने वाला। अवसाद को और-और गाढ़ा करके मन की भीतरी पर्तों में जमा देने वाला।
इस बार कुछ चार बरस बाद मेरा इलाहाबाद जाना हुआ। इलाहाबाद – वह शहर जहां मैं पैदा हुई, जहां मैंने जिंदगी के बीस बरस गुजारे। वह शहर, जहां से मेरे सुख-दुख की, हंसी और विषाद की, निजी और सामाजिक करुणा और अपमान की और पहले प्यार की सादगी और बेचारगियों की ढेरों स्मृतियां गुंथी हुई हैं। नौ साल हुए, इलाहाबाद से रोजमर्रा का वह नाता टूट गया। इधर-उधर भटकती, अपनी पहचान और जमीन तलाशती जिंदगी में फुरसत नहीं थी अपने शहर तक लौटकर जाने की। लेकिन कई बार अवसाद और अकेलेपन के बेहद निजी क्षणों में मैंने बहुत भावना से भरकर अपने शहर को याद किया था। पर इस बार बचपन की जानी-पहचानी गलियों को देखना, उनसे गुजरना बड़ा विचित्र अनुभव था। किसी भावुक आवेग और उछाल से भर देने वाला नहीं, अपने अकेलेपन में और ज्यादा धंसा देने वाला। अवसाद को और-और गाढ़ा करके मन की भीतरी पर्तों में जमा देने वाला।
प्रमोद और स्वप्नदर्शी जी की बात को आगे बढ़ाते हुए
मेरी पिछली पोस्ट छिपा लो यूं दिल में प्यार मेरा पर प्रमोद और स्वप्नदर्शी जी ने जो कहा, उस बात को समझते और पूरा-पूरा स्वीकार करते हुए मैं अपनी बात को थोड़ा आगे बढ़ा रही हूं। यह उनकी और मेरी बातों का खंडन नहीं, विस्तार है। उस लेख में 12 साल पुरानी एक घटना को याद करते हुए शायद मैं सिर्फ अपने आप से ही संवाद कर रही थी। सच के और भी जटिल कोण हैं, उस पर निगाह डालने से चूक गई। अच्छा किया प्रमोद और स्वप्नदर्शी जी ने ये बात कही, वरना शायद मैं भी समझ नहीं पाती कि सिक्के के दूसरे पहलू को अनदेखा कर मेरी बात भी उसी पाले में जा गिरती, जहां से बाहर निकलने के लिए मैं हाथ मार रही थी।
प्रमोद ने कहा, आपसी समर्पण के समन्वयन को भी ऊंचाई तभी मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है, जब समर्पित होनेवाले में स्वयं की सशक्त पहचान हो, स्वयं की पहचान के रेशे खुद जब बहुत सुलझे न हों, तो वहां समर्पण और कुछ नहीं शुद्ध ग़ुलामी होगी।
- मेरे पड़ोस में एक सुखी-सुखी नजर आने वाला एक जोड़ा रहता है। औरत चकरघिन्नी सी पति और बच्चों के चारों ओर घूमती रहती है। बड़ी समर्पित नजर आती है और खुश भी। लेकिन क्या सच सिर्फ इतना ही है ?
- मेरी मां ने पिछले 30 सालों से पति और दो बेटियों के बाहर कोई संसार नहीं देखा। हमेशा हमारे ही इर्द-गिर्द घूमती रहीं। लगता है बड़ी समर्पित हैं, दुनिया को ही नहीं, मां को खुद भी लगता है कि वो समर्पित हैं। लेकिन मैं जानती हूं और शायद अपने दिल के किसी बेहद निजी कोने में वह भी कि अगर मां के पास बाहरी दुनिया की रोशनी को उन तक पहुंचाने का कोई एक छेद भी होता तो यह समर्पण कितना टिका रहता।
- फिजिक्स की लेक्चरर मेरी एक बहन को पूरे खानदान में त्याग और चरणों में समर्पण की मिसाल माना जाता है। लेकिन उसके दिल के अंधेरे कोने में मैं घुसी हूं कई बार, जहां वह दुखी और अकेली है, लेकिन बाहरी दुनिया के सामने अपनी समर्पिता वाली इमेज को बचाए रखने के लिए वह अपने प्राण भी दे सकती है।
प्रेम में अपने अस्तित्व को बिलाकर समर्पित हो जाने की बात एक दार्शनिक अवधारणा है। यह विचार जीवन पर लागू हो, औरत और मर्द दोनों उसे अपनी जिंदगियों में उतार सकें, इसके लिए हमारे गरीब, दुखी, चोट खाए मुल्क को पता नहीं कितने सैकड़ा वर्ष का सफर तय करना होगा। मेरे आसपास सचमुच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, जिसमें ऐसा समर्पण नजर आता हो। जो इस समर्पण गीत से अभिभूत हैं, खुद उनकी जिंदगियों में भी यह नहीं है। मेरी जिंदगी में भी नहीं है। मैं किसी निजी प्रेम गीत में नहाई हुई यह बात नहीं कह रही हूं। मैं कल को किसी संबंध में जाऊं तो कौन जानता है और मैं खुद भी नहीं जानती कि उसके पीछे कितनी सारी सामाजिक, भावनात्मक असुरक्षाएं, मन, देह से लेकर आर्थिक जरूरतों तक के कितने तुच्छ और उदात्त समीकरण होंगे। ऐसे में ऐसा अमूल्य समर्पिता भाव कहीं आसमान से तो नहीं टपक सकता। सीधी सी बात है कि जिस समाज में अभाव और असुरक्षा की जड़ें इतनी गहरी हों, लगभग सभी रिश्तों के पीछे बहुत घटिया नहीं तो भी एक किस्म का जीवन को थोड़ी सुरक्षा, थोड़ा सुभीता मिल जाए, वाला कैलकुलेशन सक्रिय हो, वहां ऐसे उदात्त रिश्ते संभव नहीं हैं।
स्वप्नदर्शी ने कहा कि Is it so simple. मैं दुख और निराशा से भरकर कहती हूं, नहीं बिलकुल नहीं। कम से कम मेरे समय में तो यह असंभव की हद तक मुश्किल है।
जिस समाज का लात खाते रहने का लंबा औपनिवेशिक इतिहास न हो या जो कम से कम चेतना और कर्म के स्तर पर अभाव और गुलामी के उस मानस से बाहर आया हो, जहां कम से कम इतना तो हो लोगों का सामान्य स्वस्थ मनोविज्ञान बन सके, उनका थोड़ा स्वस्थ विकास हो सके, जहां इतनी गरीबी न हो कि एक अदद नौकरी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जिंदगी के सबसे बड़े सवाल हों क्योंकि आपका देश इस बात की कोई गारंटी ही नहीं करता कि आपको अच्छा, सम्मानजनक काम मिलेगा ही, अच्छी शिक्षा मिलेगी ही, आप बीमारी से इसलिए नहीं मरेंगे कि आपके पास पैसे नहीं या डॉक्टर को आपके इलाज से ज्यादा इस बात की चिंता हो कि वह मारुति बेच हॉन्डा सिटी कैसे खरीदे या अपने बच्चे को लॉस एंजिलिस कैसे भेजे। तो एक ऐसे समाज में जहां बड़ी मामूली इंसानी इज्जत भी मुहैया न हो, जहां हम सिर्फ इस संघर्ष में ही पूरी जिंदगी निकाल दें कि प्लीज, हमें कुत्ता नहीं, आदमी समझो तो ऐसे समाज में कुछ उदात्त समर्पित प्रेम और बहुत ऊंचा मानवीय धरातल कैसे संभव होगा?
लेकिन इन सबके बावजूद जो मैं कहना चाह रही थी और जो अब भी कह रही हूं, वह बस ये एक अन्याय और क्रूरता के प्रतिकार में हम कुछ कोमल, सुंदर विचारों का भी प्रतिकार कर देते हैं। मेरा समय इस बात की इजाजत नहीं देता कि ऐसा उदात्त समर्पण मुमकिन हो, लेकिन मुझे यह विश्वास करना चाहिए कि ऐसा होता है और ऐसा होगा। अगर बेहतर दुनिया की बातें मुगालता नहीं हैं तो यह प्रेम भी मुगालता नहीं है। औरताना बताए जाने वाले गुण सड़े हुए नहीं हैं। आप ये पॉलिटिकल स्टैंड ले सकते हैं कि उन गुणों को अपनी जिंदगी में उतार लेने को एक खास देश-काल में मुल्तवी कर दें लेकिन गुणों को ही सुपुर्द-ए-डस्टबिन न करें।
इस थोड़ा और साफ करने के लिए सिमोन द बोवुआर ने एक जर्मन पत्रकार से एक इंटरव्यू के दौरान जो कहा था, वो यहां कोट कर रही हूं –
औरतों में प्रतिद्वंद्विता और एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति नहीं होती है। सहनशीलता और धैर्य, जो एक सीमा तक तो खूबी होते हैं, लेकिन उसके बाद कमजोरी में तब्दील हो जाते हैं, भी औरतों का एक खास गुण है। औरतों में अपनी विडंबनाओं की समझ भी होती है, एक खास किस्म की सरलता और सीधापन। ये स्त्रियोचित गुण हमारे लैंगिक अनुकूलन और उत्पीड़न की उपज हैं, लेकिन यह गुण अपने आप में बुरे नहीं हैं। ये हमारी मुक्ति के बाद भी बरकरार रहने चाहिए और पुरुषों को ये गुण अर्जित करने के प्रयास करने होंगे।

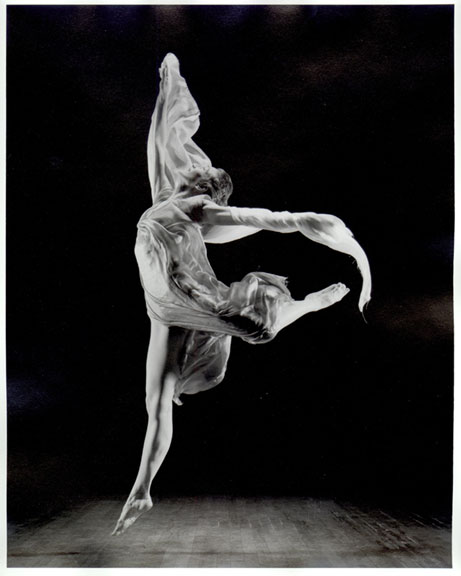

My blog is worth $0.00.
How much is your blog worth?