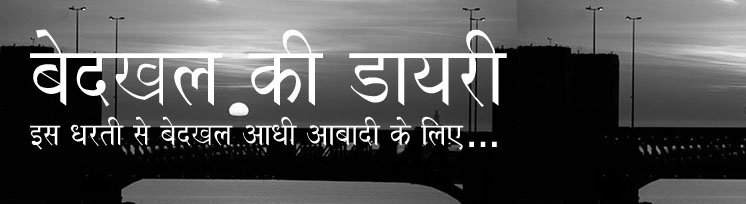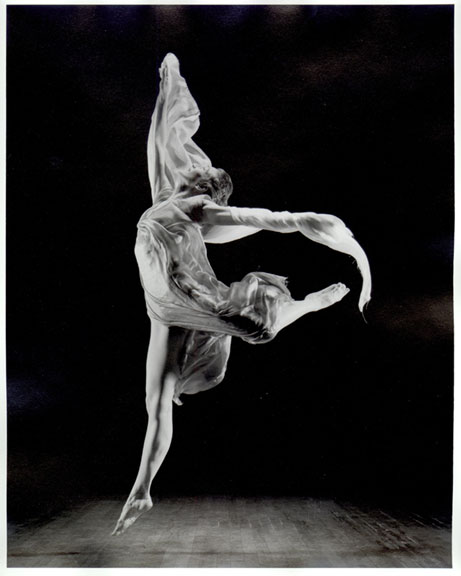अजय जी के पुरजोर इसरार पर मैंने महीनों टालने के बाद मेरी जिंदगी में सिनेमा के अनुभवों से जुड़ा ये एक पीस लिखा था, जिसे उन्होंने अपने ब्लॉग चवन्नी चैप पर लगाया है। किताबों पर लिखते हुए उसी रौ में मैंने सिनेमा पर भी कलम घसीट डाली। क्या है, कैसी है, पढ़ने वाले बताएंगे। फिलहाल इसे मैं उनकी अनुमति के बगैर ही बेदखल की डायरी पर भी चेंपे दे रही हूं।
अजय जी के पुरजोर इसरार पर मैंने महीनों टालने के बाद मेरी जिंदगी में सिनेमा के अनुभवों से जुड़ा ये एक पीस लिखा था, जिसे उन्होंने अपने ब्लॉग चवन्नी चैप पर लगाया है। किताबों पर लिखते हुए उसी रौ में मैंने सिनेमा पर भी कलम घसीट डाली। क्या है, कैसी है, पढ़ने वाले बताएंगे। फिलहाल इसे मैं उनकी अनुमति के बगैर ही बेदखल की डायरी पर भी चेंपे दे रही हूं।
एक मुख्तसर सी जिंदगी में जाने क्या-क्या ऐसा होता है कि जिनके साथ रिश्ता बनते-बनते बनता है और जो बनता है तो ऐसा कि फिर वो आपके होने का ही हिस्सा हो जाते हैं। कई बार ये रिश्ते जज्बाती और जिस्मानी रिश्तों से भी कहीं ज्यादा मजबूत और अपनापे भरे होते हैं, जो जिंदगी के हर उल्टे-सीधे टेढ़े-मेढ़े मोड़ों पर पनाह देते रहते हैं।
किताबों के बाद मेरी जिंदगी में फिल्मों की भी कुछ ऐसी ही जगह रही है। हालांकि बचपन की गलियों की ओर लौटूं तो हमारे घर में फिल्मों से रिश्ता इतना सीधा, मीठा और सुकूनदेह नहीं था, जैसाकि किताबों के साथ हुआ करता था। पापा जिला प्रतापगढ़ के जिस पंडिताऊ, सतनारायण की कथा बांचू और ज्योतिषधारी ग्रामीण परिवेश से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रगतिशील इंकलाबी वातावरण में आए थे तो यहां आने के साथ ही उन्होंने लेनिन, मार्क्स और माओ के दुनिया को बदल देने वाले विचारों से दोस्ती तो गांठ ली थी लेकिन सिनेमा और प्यार-मुहब्बत के मामलों में बिलकुल अनाड़ी थे। लेनिन की संकलित रचनाएं, क्या करें और साम्राज्यवाद– पूंजीवाद की चरम अवस्था तक तो मामला दुरुस्त था, लेकिन इससे आगे बढ़कर वो ये किसी हाल मानने को तैयार न थे कि लेनिन की कोई फ्रांसीसी प्रेमिका भी थी। उन्हें ये बात लेनिन के चरित्र को मटियामेट करने के लिए दक्षिणपंथियों द्वारा रची गई साजिश नजर आती।
फिल्मों से हजार गज का फासला बनाए रखते। उपन्यास और कविताओं से तो उनका छत्तीस का आंकड़ा था। वो इस कदर रूखे और गैररूमानी थे कि फिल्मों के नाम से ही बरजते थे। ब्याहकर इलाहाबाद आने से पहले मां ने बॉम्बे में काफी फिल्में देखी थीं, लेकिन शादी के बाद पापा ने इलाहाबाद में बस एक फिल्म दुलहन वही जो पिया मन भाए दिखाकर ये मान लिया था कि अब जिंदगी भर मां को फिल्में दिखाने का कोटा वो पूरा कर चुके हैं। मां पति की बांह से सटकर देखी उस इकलौती फिल्म का किस्सा आज भी बड़ी मुलायमियत से भरकर सुनातीं। ये बात अलग है कि बड़े होने के बाद मैंने उस फिल्म के मुतल्लिक ये फरमान जारी किया कि नई ब्याही दुल्हन को आते साथ ही इतने रूढ़िवादी टाइटल वाली फिल्म दिखाना दरअसल एक सामंती और पितृसत्तात्मक निर्णय था। मां बेलन मेरी ओर फेंककर गरजतीं, ‘बंद कर अपना ये नारीवाद,’ लेकिन ऐसा करते हुए उन्हें हंसी आ जाती।
***
पता नहीं, पापा को फिल्मों और टीवी के नाम से इतनी चिढ़ क्यों थी। तीसरी क्लास में नाना के एक पोर्टेबल ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदकर लाने तक हमारे घर में कोई टीवी नहीं था और पड़ोस की जया शर्मा के घर चित्रहार देखने जाने के लिए मां से बड़ी चिरौरी करनी पड़ती। मां इस हिदायत के साथ भेजती थीं कि पापा के आने से पहले भागकर चली आना। बगल के घर में मेरा एक कान चित्रहार और दूसरा कान पापा के आने की आहट पर लगा रहता था।
मेरी मुमकिन याददाश्त के मुताबिक मैंने कभी मां-पापा को सिनेमा हॉल जाते नहीं देखा। एक बार उनके एक दोस्त हमें सपरिवार राजा हिंदुस्तानी दिखाने ले गए थे। मैं पूरी फिल्म में आंख फाड़-फाड़कर स्क्रीन को देखती रही कि कहीं ऐसा न हो कि कोई सीन देखने से रह जाए और पापा पूरी फिल्म में तमतमाए बैठे रहे। बाद में दोस्त की बारह बजाई। मुझे यकीन था कि ये सारी नाराजगी इस वजह से थी कि एक बड़ी हो रही लड़की भी साथ बैठी थी। अकेले होते तो निश्चित ही इतना न गरजते। पर मैं खुश थी कि मुझे एक फिल्म देखने को मिली। गरज लो, बरज लो, चाहे तो कूट भी लो, पर मुझे फिल्म देखने दो। फिल्में देखना मुझे इस कदर पसंद था कि इसके लिए मैं लात खाने को भी तैयार रहती थी।
***
मात्र उन्तीस साल की जिंदगी में सिनेमा हॉल के स्याह अंधेरों की भी एक बड़ी रूमानी इमेज मेरे दिलोदिमाग पर कायम है। पहली क्लास में एक कजिन के साथ पहली दफा मैं सिनेमा हॉल गई थी। विक्रम बेताल टाइप कोई फिल्म थी, जिसमें मुकुट लगाए कोई आदमी आसमान में उड़ता था, राजकुमार सांप निगल लेता था, राजकुमारी भिखारी से शादी कर लेती थी और सुराही में से भूत निकल आता था। मैं चकित होकर बार-बार अपनी कुर्सी से उठ जाती, लगता अभी पर्दा फाड़कर अंदर घुस जाऊंगी। आंखें ऐसे बाहर निकली आती थीं कि लगता कि निकलकर अभी टपक जाएंगी। मैं महीनों वो रोमांचक मंजर नहीं भूल पाई। सपने में भी सिनेमा हॉल का नीम स्याह अंधेरा और पर्दे पर भागती-दौड़ती तस्वीरें आती थीं। कैसी अनोखी चीज थी।
इसके अलावा ज्यादातर फिल्में मैंने बॉम्बे में अपने ननिहाल की बदौलत ही देखी थीं। मां और मौसी के साथ मिथुन चक्रवर्ती और फरहा खान की पति, पत्नी और तवायफ देखी। समझ में क्या खाक आई होगी, पर पर्दे पर काफी इजहारे मुहब्बत था। कुछ अजीब-अजीब से इश्किया जुमले थे, जो सिर के पार जाते। फिल्म क्या थी पता नहीं, पर सिनेमा हॉल का वह रूमानी अंधेरा मेरे दिल में रौशन था। यूनिवर्सिटी जाने से पहले मैंने ऐसे ही कुछ-कुछ फिल्में अपने अमीर मुंबईया रिश्तेदारों के रहमो-करम पर देखी थी।
टीवी देखने की हमारे घर में कतई इजाजत नहीं थी, इसलिए घर में फिल्में देखने का सवाल ही नहीं उठता था। सिर्फ नौ बजे समाचार से पहले टीवी ऑन होता, एक बूढ़ा और नाजनीना आकर दुनिया का हाल सुनाते और फिर बेचारे बुद्वूबक्से का बटन गोल घूमता और वो चुपचाप कोने में पड़ा अपनी किस्मत को रोता था। नब्बे के दशक के पहले कुछ सीरियल जरूर देखे जाते थे। पर जैसे ही वीपी सिंह की सरकार गई, नरसिम्हा राव, डंकल आदि के साथ लोगों की जहनियत में अशांति फैलाने शांति अर्थात मंदिरा बेदी आईं और हर रोज दोपहर में स्वाभिमान सीरियल आने लगा तो सीरियलों की आमद पर भी बंदिश लग गई। टीवी चलनी ही नहीं है, बात खत्म। पापा से बहस करने का हमारा दीदा नहीं था। उनका निर्णय मां समेत हम सभी को मानना ही होता था।
फिल्मों से पापा की इस कदर नाराजगी की वजह जो बड़े होने के बाद मुझे समझ में आई वो ये थी कि दुनिया में चाहे मुहब्बत पर जितने ताले लगे हों, लड़का-लड़की को एक-दूसरे से छिपाकर सात घड़ों के अंदर रखा जाता हो, फिल्में सभी अमूमन प्यार-मुहब्बत और आशनाई के इर्द-गिर्द ही घूमती थीं। पापा को यकीन था कि छोटी बच्चियों को इस तरह के बेजा ख्यालों से दूर रखना बेहद जरूरी है वरना उनके दिमाग में तमाम ऊटपटांग चीजें आ सकती हैं, वो राह भटक सकती हैं और मुहब्बत के चक्करों में फंस सकती हैं। इसलिए घर में ऐसी किसी चीज की आमद पर सख्त पाबंदी थी। पापा के तमाम इंकलाबी विचार उन्हें ये नहीं सिखा पाए कि किसी लड़की की जिंदगी में मुहब्बत के बगीचे गुलजार होने के लिए सिनेमा की कोई जरूरत नहीं होती। जब धरती पर सिनेमा का नामोनिशान तक न था और न मुहब्बत के बाजार थे, लोग तब भी प्रेम करते थे और ज्यादा आजादी से करते थे। ये वाहियात नियम तो हमने बनाए, जलील फसीलें खड़ी कीं और फसीलें जितनी ऊंची होती गईं, मन में चोरी-छिपे मुहब्बत का दरिया उतना ही गहरा।
फिल्मों के संसार में मेरी ज्यादा आजाद घुसपैठ मेरे यूनिवर्सिटी जाने के बाद शुरू हुई। जैसे-जैसे बाहरी दुनिया में मेरी आवाजाही और दखल बढ़ने लगा, मेरी जिंदगी में मां-पापा का दखल कम होने लगा। इलाहाबाद में भी यूनिवर्सिटी के दिनों में मैं अकसर दोस्तों के साथ सिनेमा देखने चली जाती। लेकिन ये जाना सिर्फ सिनेमाई संसार में ही मेरा पहला आजाद कदम नहीं था, बल्कि यह एक हिंदी प्रदेश के छोटे शहर के बेहद कस्बाई, कटोरे जैसे दिमागों वाले लोगों की दुनिया में भी मेरा शुरुआती कदम था। द लीजेंड ऑफ भगत सिंह जैसी फिल्मों पर भी हॉल में धांय-धांय सीटियां बजतीं, कमेंट होते। लड़कियों के लिए इस कदर तरसे, उकताए और पगलाए हुए लोग थे कि पर्दे पर भगत सिंह की मंगेतर भी आ जाए तो सीट पर बैठे-बैठे आहें भरने लगते थे। और रंगीला जैसी फिल्म हो तो कहना ही क्या। शिल्पा शेट्टी यूपी-बिहार हिलातीं और इलाहाबादी मर्दानगी के दिल पर कटार चलती।
हम भी चुपचाप कोने में बैठे उर्मिला और शिल्पा की किस्मत से रश्क करते और फिल्म खत्म होने के बाद बड़े सलीके से अपने दुपट्टे संभालते सिनेमा हॉल से बाहर आते।
लेकिन फिल्मों का संसार सिर्फ शिल्पा शेट्टी और उर्मिला मार्तोंडकर तक तो सीमित था नहीं।
जीवन में देखी पहली बहुत गंभीर फिल्म जिसने भीतर-बाहर सब रौंद डाला था, वो बैंडिट क्वीन थी। यूनिवर्सिटी से एक बार मैं और मेरी एक दोस्त क्लास बंक करके सिविल लाइंस के राजकरन पैलेस पहुंचे, बैंडिट क्वीन देखने। तब मैं शायद सिर्फ साढ़े अठारह साल की थी। गेटकीपर बोला, ‘आपके देखने लायक नहीं है।’ मैं थोड़ा सा घबराई भी थी। एक बार लगा कि लौट चलें। लेकिन फिर गुस्सा भी आया। तुम क्या कोई चरित्र निर्धारक समाज के सिपाही हो, जो बताओगे कि किसके देखने लायक है, किसके नहीं। हम बोले, ‘नहीं हमें देखनी है।’ वो रहस्यपूर्ण बेशर्मी से मुस्कुराया।
‘एक सीन बहुत खराब है मैडम।’
‘कोई बात नहीं।’
फिलहाल हमें भीतर जाने को मिल गया। भीतर का नजारा तो और भी संगीन और वहशतजदा था। शहर के सारे हरामी, लफंगे जमा हो गए लगते थे। पान चबाते, गुटका थूकते, जांघें खुजाते, पैंट की जिप पर हाथ मलते, एक आंख दबाते, हम दोनों को देखकर अपने साथ के लोगों को कोहनी मारते, इशारे करते हिंदुस्तान के इंकलाबी नौजवान किसी बेहद मसालेदार मनोरंजन के लालच में वहां इकट्ठे थे। भीतर जाकर हमें थोड़ा डर लगा था। पर तभी हमरी नजर एक प्रौढ़ कपल पर पड़ी। हमने थोड़ी राहत की सांस ली। भला हो उस फटीचर सिनेमा हॉल का कि जहां नंबर से बैठने का कोई नियम नहीं था। सो हमने कोने की एक सीट पकड़ी और हम दोनो के बगल वाली सीट पर वो आंटी बैठीं और हम फिल्म देखने लगे।
मैंने जिंदगी में बहुत सी तकलीफदेह फिल्में देखी हैं, पर वो मेरी याद में पहली ऐसी फिल्म थी, जिसका हर दृश्य हथौड़े की तरह मेरे दिलोदिमाग पर नक्श होता जा रहा था। वो दर्द और बदहवासियों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला जान पड़ती थी। जैसे-जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाती, लगता मैं सुलगते अंगार निगल रही हूं। रोते-रोते आंखें सूज आईं। आवाज गले में ही अटकी रही। मैं कांपती, बदहवास और संज्ञाशून्य सी उस फिल्म को देखती रही। फूलन देवी का दर्द अपनी ही धमनियों में दौड़ता सा लगा था।
हमसे आगे वाली रो में बैठे दो लड़के बीच-बीच में मुड़-मुड़कर हम दो लड़कियों को देखते रहते और बेहयाई से मुस्कुराते थे। फिल्म के सबसे तकलीफदेह हिस्सों पर हॉल में दनादन सीटियां बजीं, गंदे जुमले उछले और मर्दों की बेशर्म सिसकारियों की आवाजें आती रहीं। मेरी उम्र तब सिर्फ साढ़े अठारह साल थी। दुनिया की कमीनगियों से ज्यादा वास्ता न पड़ा था और न ही लात खाते-खाते मैं पत्थर हो गई थी। एक छोटा बच्चा जरा सी तेज आवाज से भी हदस जाता है और तीस पार कर हम इतने संगदिल हो चुके होते हैं कि गालियों और लात-जूतों पर भी आंसू नहीं बहाते। तकलीफें हमारे खून में बस जाती हैं, हम उनके साथ रहने-जीने के आदी हो जाते हैं। लेकिन तब तक तकलीफों से मेरी ऐसी आशनाई नहीं हुई थी। वो मेरी तब तक की जिंदगी का सबसे दुखद क्षण था। मैं इतनी ज्यादा तकलीफ महसूस कर रही थी कि उसी क्षण मर जाना चाहती थी। मुझे लगा कि मैं खड़ी होकर जोर से चीखूं। सबकी हत्या कर दूं। फूलन देवी पर्दे से बाहर निकल आए और उन ठाकुरों के साथ-साथ हॉल में बैठे सब मर्दों को गोली से उड़ा दे। जून, 99 की वो दोपहर मेरे जेहन पर ऐसे टंक गई कि वक्त का कोई तूफान उसे मिटा नहीं सका। आज भी आंख बंद करती हूं तो वो दृश्य फिल्म की रील की तरह घूमने लगता है।
फिल्म खत्म होने के बाद जब हम बाहर निकले तो मेरी आंखें सूजकर लाल हो गई थीं। मैं अब भी मानो किसी सपने में चल रही थी। चारों ओर लोग ठहाके लगा रहे थे, आपस में भद्दे मजाक कर रहे थे। हमें देखकर आंख दबा रहे थे।
कैसी है ये दुनिया? कैसा इंसान रचा है हमने? वो फूलन तो एक थी, लेकिन इन सब मर्दों की बीवियां, उनकी बहनें, माएं सबकी जिंदगी फूलन जैसी ही है। सबके हाथ में एक-एक बंदूक होनी चाहिए और उड़ा देना चाहिए इन सब हरामियों को।
***
मैंने जिंदगी में सबसे धुंआधार फिल्में बंबई में देखीं। हॉस्टल भी किस्मत से ऐसी जगह था कि दसों दिशाओं में दस कदम पर इरोज, लिबर्टी, मेट्रो, स्टर्लिंग, न्यू एंपायर, न्यू एक्सेलसियर और थोड़ी ज्यादा दूर रीगल थिएटर थे। 2001 के बाद से मेरे बॉम्बे रहने के दौरान जितनी भी फिल्में आईं, लगभग सब मैंने थिएटर में देखीं। वहां रिलीज होने वाली फिल्मों का कैनवास जरा ज्यादा व्यापक था। अंग्रेजी फिल्में, ऑस्कर विनर फिल्में, बंगाली फिल्में, समांतर सिनेमा और मल्टीलिंग्वल मल्टीप्लेक्स फिल्में सभी कुछ देख डालीं, यहां तक कि एक्सक्यूज मी, स्टाइल और मस्ती टाइप की बेहद थर्ड क्लास डबल मीनिंग फिल्में भी मेरे देखने से नहीं छूटीं। जिस्म, मर्डर, पाप और हवा जैसी मूर्ख फिल्में भी। उस समय इस तरह भटक-भटककर फिल्में देखना आवारगी की ही एक इंतहा थी। प्रणव को भी फिल्मों का शौक था। इसलिए हम साथ कहीं और जाएं न जाएं, पर फिल्में जरूर देखते थे। उसके अलावा भी मैं कभी देखने की मौज में, कभी अवसाद और अकेलेपन में तो कभी मुहब्बत की रूमानियों में सिनेमा हॉलों के अंधेरों में पनाह लेती थी। धकाधक फिल्में देखती थी। आजादी का नया-नया स्वाद था, सिनेमाई कल्पनाओं की तारीक रौशनियों से पर्दे उठने शुरू ही हुए थे, दफ्तर का जिन्न नहीं था, समय की मारामारी नहीं और रुपहले पर्दे का रोमांस तो था ही। इन तमाम कारणों से मैं फिल्मों और फिल्में मुझसे करीबी हुए।
बॉम्बे में हॉस्टल की लड़कियों के साथ भी मैंने कई बार फिल्में देखीं, लेकिन बहुत कम। फिल्म देखते समय मेरे रोने से वो हैरतजदा होतीं और मेरा मजाक उड़ाती थीं। इसलिए मैं ज्यादातर अकेले ही फिल्म देखती थी। हां, किसी फिल्म में प्यार-मुहब्बत का इजहार अगर खासे इरॉटिक अंदाज में हो तो हॉस्टल में उस फिल्म की अच्छी माउथ पब्लिसिटी हो जाती थी और सब मरती-मराती फिल्म देखने पहुंच जातीं। रोमांटिक फिल्मों की खासी मांग थी, जिनमें सच्चा प्यार दिखाया जाता, हीरो हिरोइन के लिए जान देने को तैयार हो जाता। बरसों गुजर जाते, वे मिल न पाते तब भी मन ही मन प्यार करते रहते थे। हम लड़कियां ऐसी फिल्में देखकर आंसू बहातीं। हम ये मान लेते कि पर्दे पर प्रीती जिंटा नहीं हम ही हैं और शाहरुख खान ने हमारे लिए ही इतने बरस गुजार दिए। असल जिंदगियों में प्यार कहीं नहीं था। सिर्फ कुछ टाइम पास था, कैलकुलेशन था, बहुत पेटी इंटरेस्ट थे, मूर्खतापूर्ण मुहब्बती भंगिमाएं थीं, भावुक, कुंदजेहन इमोशंस थे। सब था पर प्यार नहीं था। और ऐसे में साथिया, देवदास और वीर जारा देखकर हम अपनी जिंदगी के अभाव भरते थे। हर दृश्य के साथ हमारे चेहरे की बदलती भंगिमाएं बताती थीं कि हमने उस फिल्म को कितना आत्मसात कर लिया था। सभी का ये हाल था। फिल्में हमारे अभावों और कुंठाओं पर मरहम लगाती थीं। हम प्रीती जिंटा के साथ खुश और दुखी होते और फिर उसी बेरहम चिरकुट कैलकुलेशनों वाली दुनिया में लौट आते।
****
तब फिल्में देखने का एक अजीब सा नशा था। आज भी है। सिनेमा हॉल के रूमानी अंधेरे में बैठने का। पर अब उस तरह नहीं देखती। अब तो किसी फिल्म के आजू-बाजू, दाएं-बाएं, ऊपर-नीचे कहीं भी बी एच ए डबल टी लिखा हो तो गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो लेती हूं। वो फिल्म नहीं देखनी, चाहे धरती सूरज को छोड़ चंद्रमा का ही चक्कर क्यों न लगाने लगे।
इतने सालों में सिनेमा की टूटी-फूटी जो भी समझ बनी, उसके साथ फिल्में देखने का दायरा बढ़ा है और सलीका भी। अब मैं थिएटर में जाकर बहुत कम फिल्में देखती हूं। रॉक ऑन, माय नेम इज खान, वेक अप सिड एंड फिड, यहां तक कि थ्री इडियट्स टाइप मध्यवर्गीय चेतना संसार में सुनामी ला देने वाली फिल्में भी मैं भूलकर भी थिएटर में देखने नहीं जाती। गलती से पा देख ली थी और पूरे समय यही सोचती रही कि ये फिल्म बनाने वाले दर्शक को मूर्ख, गधा, आखिर क्या समझते हैं। वो कुछ भी उड़ेलते रहेंगे और हम भावुक होकर लोट लगाएंगे।
थ्री इडियट्स के युग परिवर्तनकारी विचारों से लहालोट होने वाले, पा देखते हुए भावुक होकर आंसू बहाने वाले और वेक अप सिड की जेंडर सेंसिबिलिटी को कोट करने वाले हिंदी सिनेमाई दर्शकों की सेंसिबिलिटी के बारे में जरा थमकर, रुककर सोचने की जरूरत महसूस होती है। ये फिल्में अब मुझे छूती नहीं, उल्टे इरीटेशन होता है, गुस्सा आता है कि सौ रुपए फूंक दिए। बीच-बीच में कुछ फिल्में ऐसी भी आती हैं कि आपका ज्यादा मूड खराब न हो, जैसे पिछले साल जोया अख्तर की लक बाय चांस थी या इस साल इश्किया। ये फिल्में ऐसी खराब नहीं हैं, पर बर्गमैन, कुरोसावा, बहमन घोबादी, मखमलबाफ, मजीदी, वांग कारवाई, त्रूफो, फेलिनी, बुनुएल, स्पीलबर्ग, फासबाइंडर, त्रोएसी और अभी एक नए इस्राइली निर्देशक इरान कोलिरिन की फिल्में देखने के बाद सिनेमा से आपकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं।
सिनेमा की थोड़ी समझ और तमीज आने और इस माध्यम की ऐसी अनोखी कलाकारी, इतना ताकतवर इस्तेमाल देखने के बाद लगता है कि सिनेमा सिर्फ एक चोट खाए, पिछड़े, दुखी मुल्क के लोगों के अभावों, कुंठाओं को बेचने और भुनाने का माध्यम भर नहीं है। ये अपने भीतर इतनी ताकत समेटे है कि किसी इंसान का जमीन-आसमानी बदलाव कर सकता है, दिल में छेद कर सकता है, हिला सकता है, बना और मिटा सकता है। ये मन और सोच की दुनिया बदल सकता है।
इसलिए अब मैं उस सिनेमा की तलाश में रहती हूं कि जो मन में छेद करे और पहले के छेदों को भर सके। जो अभावों पर मरहम न लगाए, पर उसे समझने और उसके साथ गरिमा से जीने का सलीका सिखाए। जो संसार की एक ठीक-ठीक, भावुक नहीं, पर संवेदनशील समझ पैदा करे।
निश्चित तौर पर हिंदी फिल्में ये काम नहीं करतीं।
 हम कौन हैं? हम क्यों हैं? क्या है हमारे होने का मतलब? हम क्यों होना चाहते हैं? क्यों होना चाहिए हमें? जो न हों तो किसका क्या बिगड़ता है? क्या आता है, क्या चला जाता है? हमारा ये होना हमारे लिए है या कि किसके लिए? इस सृष्टि के एक कण से बनी मैं, मेरे होने का मतलब क्या है? क्या पता है मुझे? क्या चाहती हूं अपनी जिंदगी से? ये जो हम हैं इस सृष्टि में, क्यों?
हम कौन हैं? हम क्यों हैं? क्या है हमारे होने का मतलब? हम क्यों होना चाहते हैं? क्यों होना चाहिए हमें? जो न हों तो किसका क्या बिगड़ता है? क्या आता है, क्या चला जाता है? हमारा ये होना हमारे लिए है या कि किसके लिए? इस सृष्टि के एक कण से बनी मैं, मेरे होने का मतलब क्या है? क्या पता है मुझे? क्या चाहती हूं अपनी जिंदगी से? ये जो हम हैं इस सृष्टि में, क्यों?